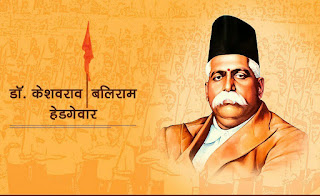संघ संस्थापक डॉ० केशवराव बलिराम हेडगेवार
डॉ० हेडगेवार का जन्म युगाब्द 4991 की चैत्र शुक्ल अर्थात दिनांक 01 अप्रैल, 1889 ई० को नागपुर के एक गरीब वेदपाठी परिवार में हुआ था। पुरोहित की आजीविका चलाने वाला उनका परिवार नागपुर की एक पुरानी बस्ती में निवास कर रहा था। घर का वातावरण आधुनिक शिक्षा और देश के सार्वजनिक जीवन से सर्वथा अछूता था। उम्र के आठवें वर्ष में ही उनके मन में ऐसा विचार आया कि इंग्लैण्ड की रानी विक्टोरिया का राज्य पराया है और उसके साठ साल पूरे होने की खुशी में जो मिठाई बाँटी गयी, उसे खाना हमारे लिए लज्जा की बात है। और मिठाई का वह दोना उन्होंने एक कोने में फेंक दिया। चार साल बाद एडवर्ड सप्तम का राज्याभिषेक-समारोह जब बड़े ठाठ-बाट से मनाया गया तब उसमें भी केशव ने भाग नहीं लिया। बालक केशव ने कहा "पराये राजा का राज्याभिषेक समारोह मनाना हम लोगों के लिए घोर लज्जा की बात है।" विद्यालय में पढ़ते समय नागपुर के सीताबर्डी के किले पर अंग्रेजों के झण्डे ‘युनियन जैक' को देखकर उन्हें बड़ी बेचैनी होती थी और मन में लालसा जगती थी कि उसके स्थान पर भगवा झण्डा फहराया जाए। एक दिन एक अनोखी कल्पना उनके मन में उभरी कि किले तक सुरंग खोदी जाए और इसमें से चुपचाप जाकर उस पराये झण्डे को उतारकर उसकी जगह अपना झण्डा लगा दिया जाये। तद्नुसार उन्होंने अपने मित्रों सहित सुरंग खोदने का काम शुरू भी किया था।
वे जब नागपुर के नीलसिटी हाईस्कूल में पढ़ रहे थे, तभी अंग्रेज सरकार ने कुख्यात रिस्ले सक्र्युलर जारी किया। इस परिपत्र का उद्देश्य विद्यार्थियों को स्वतन्त्रता-आन्दोलन से दूर रखना था। नेतृत्व का गुण केशवराव हेडगेवार में विद्यार्थी अवस्था से ही था। पाठशाला के निरीक्षण के समय उन्होंने प्रत्येक कक्षा में निरीक्षक का स्वागत 'वन्देमातरम्' की घोषणा से करने का निश्चय किया और उसे सफलता के साथ पूरा कर दिखलाया। विद्यालय में खलबली मच गयी, मामला तूल पकड़ गया और अंत में उस सरकार-मान्य विद्यालय से उन्हें बाहर निकाल दिया गया। फिर यवतमाल की राष्ट्रीय शाला में उन्होंने मैट्रिक की पढ़ाई की, किन्तु परीक्षा देने से पूर्व ही वह शाखा भी सरकारी कोप का शिकार हो गयी। 'काल' और 'केसरी' सरीखें समाचार-पत्रों के आग उगलते लेख, लोकमान्य तिलक के गरजते भाषण, अंग्रेजी साम्राज्यवाद का दमनचक्र, बंग-भंग के विरोध में उभरा उग्र आन्दोलन, क्रान्तिकारियों के साहस भरे कार्य और उनका बलिदान आदि बातें, केशवराव पर असर करतीं गयी। उन्होंने सन् 1910 में कलकत्ते के नेशनल मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरी की शिक्षा के लिए प्रवेश लिया ताकि उनका बंगाल के क्रान्तिकारियों से सम्पर्क आ सके और बाद में वह वैसा ही कार्य विदर्भ में कर सकें। वहाँ पुलिनबिहारी दास के नेतृत्व में 'अनुशीलन समिति' नामक क्रान्तिकारियों की एक टोली काम कर रही थी। इस समिति के साथ केशवराव का गहरा संबंध स्थापित हुआ और वे उसके अंतरंग में प्रवेश पा गये। कलकत्ते के मेडिकल कॉलेज में पाँच वर्ष का पाठ्यक्रम पूरा कर वह 'डाक्टर' बन गये। इस पाँच वर्ष के कालखण्ड में भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में अगुवाई करने वाले नेताओं का उन्होंने स्नेह प्राप्त किया। स्थान-स्थान के क्रान्तिकारियों से उनकी घनिष्ठता बढ़ी और उन सभी को शस्त्रास्त्र इधर-से-उधर गुपचुप पहुँचाने के काम में उनकी सावधानी, संयम, योजकता आदि गुणों का परिचय प्राप्त हुआ। इस काम में प्रान्त और भाषा की अड़चन उनके आड़े नहीं आयी। बंगाली भाषा उन्होंने भली-भाँति सीख ली थी और अनेक लोगों से मैत्री-संबंध जोड़ लिए थे। बाढ़, महामारी आदि संकटों के समय उन्होंने अपने तरुण मित्रों को साथ लेकर परिश्रमपूर्वक नि:स्वार्थ सेवा की। केशवराव जब डॉक्टरी की उपाधि प्राप्त कर नागपुर वापस आये और लोकमान्य तिलक के अनुयायी बनकर कांग्रेस के आन्दोलन में कूद पड़े। लोकमान्य तिलक के प्रति डॉक्टर साहब की इतनी भक्ति थी कि एक बार जब कलकत्ते की एक जनसभा में एक वक्ता ने तिलक जी को अपशब्द कहे तो डॉक्टर साहब ने मंच पर जाकर उसे ऐसा जोरदार थप्पड़ मारा कि उसका थोबड़ा लाल हो गया। वे पूर्ण स्वतन्त्रता के पक्षधर थे और अपनी यह बात बड़े आग्रह के साथ रखा करते थे। जहाँ भी अवसर मिलता, वे अत्यन्त उग्र एवं उत्तेजक भाषण दिया करते थे। डॉक्टर साहब ने काँग्रेस के अन्दर ही उग्र विचारों का एक गुट खड़ा किया था। सन् 1919 का काँग्रेस-अधिवेशन अत्यन्त तनावपूर्ण वातावरण में अमृतसर में सम्पन्न हुआ और अगले वर्ष का अधिवेशन नागपुर में करने का निश्चय किया गया। अमृतसर के अधिवेशन में डा० हेडगेवार उपस्थित थे। सन् 1915 से 1920 तक नागपुर में रहते हुए डॉक्टर साहब राष्ट्रीय आन्दोलनों में अत्यन्त सक्रिय रहे। प्रवास, सभा, बैठक आदि कार्यक्रमों में वे सदा व्यस्त रहा करते थे। किन्तु तरुणों में पूर्ण स्वतन्त्रता की आकाँक्षा धधकाने पर वे विशेष ध्यान देते थे। हाथ में लिए काम में अपने आप को झोंक देने, सहयोगियों को जोड़ने और नि:स्वार्थ भाव से काम करने के उनके गुणों के कारण नेता लोगों को उनका सहयोग अत्यन्त मूल्यवान् प्रतीत होने लगा। स्वयं को जो लगता था उसे बिना लाग-लपेट के बड़े नेताओं के सामने रखने का साहस भी डॉक्टर जी में था। सन् 1920 के नागपुर काँग्रेस अधिवेशन में उनके इन गुणों का अनुभव सबको हुआ और मतभेदों के होते हुए भी संस्था के अनुशासन का पालन करने का उनका एक और अनुकरणीय गुण भी सबको देखने को मिला। अधिवेशन में आए साढ़े चौदह हजार प्रतिनिधियों की सुख सुविधा और अन्य व्यवस्थाएँ संभालने के लिए डॉ०ल०वा पराङजपे और डॉ० हेडगेवार के नेतृत्व में एक स्वयंसेवक दल का गठन किया गया था। यह सारी जिम्मेदारी उन्होंने इतने अच्छे ढंग से निभाई कि वे सभी की प्रशंसा के पात्र बन गये ।
सन् 1922 से 1925 तक के तीन वर्षों का वह काल उनके गहरे विचार-मंथन का काल कहा जा सकता है। तत्कालीन परिस्थितियों को देखते हुए डॉक्टर साहब इस व्यावहारिक निष्कर्ष पर पहुँचे कि यदि अलगाववाद पर चलने वाले मुस्लिम कट्टरपंथियों तथा उनको उकसाने वाले अंग्रेजों का सफलतापूर्वक सामना करना है तो उसका एकमात्र उपाय यह है कि यहाँ के वास्तविक राष्ट्रीय समाज यानि हिंदू समाज को संगठित किया जाय। उनकी दृष्टि में समस्त समस्याओं को सुलझाने का एकमेव मार्ग भी यही था।
डाक्टर साहब जिन दिनों अपना जीवनकार्य तय कर रहे थे, उन दिनों हिंदू राष्ट्र का विचार वायुमण्डल में पहले से ही विद्यमान था। सार्वजनिक कार्य करने के जो तरीके उन दिनों प्रचलित थे और स्वतन्त्रता प्राप्ति के लिए जिस प्रकार के प्रयत्न किए जा रहे थे, उनसे अलग हटकर उन्होंने अपनी प्रतिभा से 'शाखा' की एक नयी पद्धति खोज निकाली। अनुशासनपूर्वक नित्य चलाई जा सकने वाली इस पद्धति में स्थायी संस्कार देने की क्षमता थी। इस पद्धति की मुख्य बात यह थी कि नियमित रूप से कुछ समय देने की लोगों को आदत डाली जाये और उनके मन की धीरे-धीरे राष्ट्र के लिए ही तन-मन-धन पूर्वक जीने की तैयारी करवायी जाये। संगठन की अपनी यह कल्पना उन्होंने अनेक लोगों को बतायी और उस पर उनसे चर्चा भी की। किन्तु उन दिनों के बड़ी आयु के सार्वजनिक कार्यकर्ताओं को वह ठीक से समझ में नहीं आयी। अंत में मुट्ठी भर तरुणों की एक बैठक बुलाकर डॉक्टर साहब ने घोषणा कर दी कि "हम संघ की स्थापना कर रहे हैं।" वह युगाब्द 5027 अर्थात् सन् 1925 की विजयादशमी का पवित्र दिन था। इस पहली बैठक में संघ स्थापना की घोषणा अवश्य हुई, किन्तु नाम तय नही हुआ। फिर भी, ऐतिहासिक महत्व की बात यह कि उस दिन संघ-कार्य का बीज बोया गया। लम्बे चिन्तन के पश्चात् उन्होंने अपने जीवन-कार्य का शुभारम्भ पुरुषार्थ की प्रेरणा देने वाले उस राष्ट्रीय पर्व पर किया। उस समय डॉक्टर साहब की उम्र मात्र 36 साल थी। तथा उसके पास न पैसा है, न कोई साधन; पीछे न कोई बड़ा नेता है और न हिंदू राष्ट्र के विचार को जनता में मान्यता ही है। उल्टे, परिस्थिति पूरी तरह विपरीत है। हिंदू समाज अनेक जाति, पंथ, भाषा और प्रान्तों में विभाजित होने के कारण दीर्घकाल से गुलामी में रहता आ रहा था। हिंदू राष्ट्र की बात समझना तो दूर, वैसा बोलना भी निरा पागलपन माना जाता था।
सन् 1925 की विजयादशमी के दिन संघ की स्थापना तो हो गयी, किन्तु उसकी पूरी कार्यपद्धति तब तक निश्चित नहीं हुई थी। सबसे पहले नाम निश्चित हुआ-'राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ' नामकरण की बैठक में उन्होंने स्पष्ट रूप से समझाया कि हिंदुस्थान में हिंदुओं का संगठन राष्ट्रीय ही कहलायेगा। ‘स्वयंसेवक' शब्द की भी उन दिनों सामाजिक जीवन में बड़ी दयनीय स्थिति थी। स्वयंसेवक का अर्थ माना जाता था नेताओं द्वारा बताए गए ऐसे छोटे-मोटे काम करने वाला, जिनमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। वे 'राष्ट्रीय' और 'स्वयंसेवक ' दोनों शब्दों को एक भिन्न अर्थ देने में सफल हुए। ऐसी कल्पना उन्होंने प्रारम्भ से ही प्रचलित की कि स्वयं की प्रेरणा से देश के लिए कष्ट उठाने वाला, नि:स्वार्थ बुद्धि से समय देने वाला, देश के काम के लिए अगुवाई करने वाला और सब कुछ समर्पण करने के लिए तैयार रहने वाला, अनुशासन का बन्धन स्वेच्छा से स्वीकार करने वाला तथा तीक्ष्ण बुद्धि से सम्पन्न, देशभक्ति से भरा हुआ कार्यकर्ता ही स्वयंसेवक है। डॉक्टर साहब ने 'संघ' शब्द का प्रयोग विशुद्ध राष्ट्रहित से प्रेरित होकर काम करने वाले नि:स्वार्थ एवं अनुशासनबद्ध लोगों के संगठन के लिए किया। यह शब्द इतना प्रचलित हुआ कि आज संघ कहते ही 'राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ' का चित्र ही लोगों की आँखों के सामने उभरता है। 'संघ' कहने पर समस्त हिंदू-समाज को समेटकर चलने वाली व सारे राष्ट्र को व्यापने वाली हिंदू-शक्ति का बोध होता है।
प्रारम्भ में न तो अपना कोई संविधान बनाया, न नियम व पदाधिकारी, और न निधि की ही व्यवस्था की। उन्होंने कार्यालय और कागज-पत्र आदि व्यवस्थित करने की कभी चिन्ता नहीं की, क्योंकि उनकी दृष्टि में सबसे अधिक महत्व मनुष्य का और उस मनुष्य पर डाले जाने वाले उन्नत संस्कारों का था। इस काम को करने के लिए उन्होंने 10-15 वर्षों के अपने सार्वजनिक जीवन के अनुभवों से सीख लेकर अपनी प्रतिभा से एक बिल्कुल ही अनोखी कार्यपद्धति का विकास किया। विशिष्ट कार्यपद्धति द्वारा मनुष्यों को जोड़ने व उन्हें संस्कारित करने पर उनका मुख्य ज़ोर था। किन्तु संघ -कार्य का आरम्भ रोज की शाखा से नहीं हुआ। उस समय मुख्यत: बैठक के रूप में ही सारे सदस्य एकत्रित होते थे। शारीरिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए वे सब किसी न किसी व्यायामशाला में जाते थे। किन्तु कुछ ही दिनों बाद नागपुर के महाल नामक भाग में संघ की पहली दैनिक शाखा शुरू की गयी। डॉक्टर साहब ने शाखा के माध्यम से बाल, तरुण और प्रौढ़ों को एकत्रित करने और उन्हें संस्कारित करने पर सबसे अधिक बल दिया। संघ की स्थापना के बाद जो पन्द्रह वर्ष उन्हें मिले उस अवधि में नागपुर में तैयार हुए कार्यकर्ता न केवल विदर्भ और महाराष्ट्र में, अपितु भारत के और भी अनेक प्रान्तों में गये और वहाँ संघ-कार्य का बीज बोया। सन् 1940 के संघ-शिक्षा वर्ग में पंजाब, सिंध, दिल्ली, उत्तरप्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक, बंगाल, तमिलनाडु आदि अनेक प्रान्तों से स्वयंसेवक आए थे। इन स्वयंसेवकों को विदाई देते हुए दिनांक 09 जून, 1940 के दिन अपनी बीमारी की अवस्था में दिए गए अपने जीवन के अन्तिम भाषण में डॉक्टर साहब ने एक बड़ा ही अर्थपूर्ण वाक्य कहा –“मैं अपनी आँखों के सामने हिंदू-राष्ट्र का छोटा रूप देख रहा हूँ।"
1940 तक किए गए प्रयत्नों के फलस्वरुप सब प्रान्तों में संघ की शाखाएँ शुरू हो गई हैं। स्वाभाविक ही इस कारण वह हौआ समाप्त हो गया जो प्रांत, भाषा, जाति, पंथ आदि के भेदों के आधार पर खड़ा किया जाता था। हिन्दुत्व की समान भावना के आधार पर संगठन खड़ा करने के राष्ट्रीय संकल्प को पूरा कर दिखाने का मार्ग अब खुल गया था। डॉक्टर साहब ने यह विश्वास निर्मित करने में सफलता प्राप्त कर ली थी कि संघ के मंत्र और संगठन के तंत्र का निष्ठापूर्वक पालन करने से निश्चय ही सफलता मिलती है।
डॉक्टर साहब ने स्वयंसेवकों को बताया कि भगवाध्वज हमारा गुरु है, अत: प्रतिवर्ष गुरुपुर्णिमा के दिन इसका पूजन कर दक्षिणा-समर्पण करना चाहिए। अनोखा आविष्कार ही मानना पड़ेगा कि गुरु के स्थान पर किसी व्यक्ति को न रखकर भारतीय-संस्कृति के प्रतीकरूप भगवा ध्वज को स्थापित किया। इस पद्धति के द्वारा उन्होंने संगठन को व्यक्ति-पूजा और उससे उत्पन्न होने वाले अन्य दोषों से बचा लिया। संगठन के लिए दक्षिणा-पद्धति को स्वीकार कर जहाँ उन्होंने उसे स्वालम्बी रहने का मार्ग दिखाया, वहीं धनवानों के अनिष्ट दबाव से मुक्त रहने का उपाय भी दे दिया। इस पद्धति का एक और उत्तम पक्ष यह है कि इससे स्वयंसेवकों के मन में अधिकाधिक समर्पण की भावना का विकास किया जा सका।
विजयादशमी, मकर-संक्रान्ति, वर्ष-प्रतिपदा, गुरु-पूर्णिमा व रक्षाबन्धन के परम्परागत उत्सव संघ-शाखाओं द्वारा मनाये जाने हेतु चुने गये। इन उत्सवों को नया राष्ट्रीय और सामाजिक अर्थ दिया गया और उन्हें जनसम्पर्क का प्रभावी माध्यम बनाया गया। इन पाँच परम्परागत उत्सवों के साथ डॉक्टर साहब ने 'हिंदू-साम्राज्य दिवस' का छठा उत्सव भी प्रचलित कर स्वयंसेवकों व समाज के सामने असंदिग्ध रूप से यह बात रखी कि संघ क्या करना चाहता है। उनकी दृष्टि में ‘हिन्दुओं के साम्राज्य' की कल्पना यह थी कि हिंदुओं का सांस्कृतिक प्रभाव भारत के बाहर भी पड़े और संसार के लोग हिंदुओं के श्रेष्ठ जीवन-मूल्यों का अनुसरण करें। 'हिंदू साम्राज्य दिनोत्सव' प्रारम्भ करने का यही हेतु था और यही है भारत का राष्ट्रीय ध्येय।
डॉक्टर साहब प्रार्थना और प्रतिज्ञा की संस्कार-क्षमता अच्छी तरह जानते थे, इसलिए उन्होंने इनको भी अपनी कार्यपद्धति में स्थान दिया। प्रतिज्ञा दिलाने का पहला कार्यक्रम मार्च, 1928 में नगर से दूर एक शान्त, सुरम्य स्थान पर सम्पन्न हुआ जिसमें 99 स्वयंसेवकों ने भाग लिया। इस पहली टोली के अधिकांश स्वयंसेवकों ने संघ का कार्य अक्षरश: जीवन भर निभाया। उनमें से जो अभी जीवित हैं वे आज भी काम में जुटे हुए हैं।
प्रारम्भ में संघ की प्रार्थना में एक छन्द हिंदी का और एक मराठी का था और महाराष्ट्र से बाहर की शाखाओं में भी यही प्रार्थना होती थी। पर जब संघ-कार्य कई प्रान्तों में फैल गया, तब डॉक्टर साहब के मन में ऐसी प्रार्थना तैयार करने का विचार आया जो देशभर में सहजता से कही जा सके और जिसके द्वारा स्वयंसेवकों को संघ के विचारों और ध्येय का नित्य स्मरण होता रहे। साथ ही, किसी भी सम्प्रदाय के व्यक्ति को उसे कहने में कोई अड़चन न मालूम पड़े। इस दृष्टि से सन् 1939 में नागपुर से 30 मील दूर सिंदी नामक स्थान पर संघ के प्रमुख कार्यकर्ताओं की एक बैठक हुई। उसमें प्रार्थना तथा कार्यपद्धति पर विस्तार से विचार हुआ। उनके बाद संघ में संस्कृत-भाषा में रचित प्रार्थना और आज्ञाएँ हुई।
यद्यपि प्रधानत: डॉक्टर साहब ही संघ की कल्पना और कार्यपद्धति को साकार रूप दे रहे थे और उसके विस्तार का भार भी परिश्रमपूर्वक वहन कर रहे थे, तथापि प्रारम्भ के वर्षों में उनके पास संघ का कोई पद अधिकृत रूप से नहीं था। अपनी विशिष्ट भूमिका के कारण वे संघ के स्वयंसिद्ध नेता थे। जैसे-जैसे कार्य बढ़ने लगा, वैसे-वैसे उनके सहयोगियों को अनुभव होने लगा कि संघ का सूत्रबद्ध सङचालन करने के लिए एक सर्वोच्च पद की स्थापना करना आवश्यक है और उस पद पर डॉक्टर जी को ही बैठाया जाना चाहिए। तदनुसार नवम्बर, अवश्य निपटाना पड़ता था। 1929 में संघ के कार्यकर्ताओं ने निश्चय किया कि डॉक्टर साहब को इसके बाद 'सरसंघचालक' माना जाये और देश की सब शाखाएँ उनके मार्गदर्शन के अनुसार चलें। सहयोगियों का यह आग्रह उन्होंने स्वीकार तो कर लिया, किन्तु अनिच्छा से; क्योंकि वह संगठन-कार्य पद के कारण नहीं, ध्येय निष्ठा से करने की परम्परा डालना चाहते थे। इसलिए संघ में पद के लिए कोई झगड़ा नहीं होता। पद पर बैठने से व्यक्तिगत लाभ तो कुछ होता ही नहीं, उल्टे अपेक्षा यही रहती है कि अधिकार-पद पर बैठा व्यक्ति अधिक कार्य करे।
अनेक स्थानों पर संघ के प्रभावी कार्यक्रम होने लगे। संघ के संचलन, घोष-पथक तथा आकर्षक शारीरिक कार्यक्रमों आदि के कारण अनेक लोग संघ की ओर आकर्षित होते थे। सम्भवत: ईष्या के कारण सन् 1932 में मध्यप्रदेश शासन ने एक परिपत्र निकालकर सरकारी कर्मचारियों को संघ में जाने की मनाही कर दी। एक बार और 1934 में सरकार ने स्थानीय स्वायत्त संस्थाओं को एक पत्रक प्रसारित कर सलाह दी कि वे अपने कर्मचारियों को संघ के कार्यक्रमों में जाने से रोकें । महात्मा गाँधी जी सन् 1934 में वर्धा में संघ का शीतकालीन शिविर देखने आए थे और उन्होंने बाद में डॉक्टर साहब से मिलकर संघ की नीति और कार्य-पद्धति के संबंध में जानकारी प्राप्त की थी। सन् 1939 में हिन्दू युवक परिषद् के लिए पूना गये थे। सम्मेलन में पहुँचने से पूर्व चायपान आदि के लिए वे कुछ समय आचार्य अत्रे के यहाँ रुके थे। इस सम्बन्ध में आचार्य अत्रे ने बाद में लिखा कि डाक्टर साहब सरीखा नेता उनके घर आने वाला है, इस बात का पहले उनके मन पर बड़ा दबाव था। पर जब वे प्रत्यक्ष आये, तो उनका बोलना-चालना देखकर वह दबाव एकदम दूर हो गया और ऐसा लगा मानो कुटुंब के ही कोई बड़े व्यक्ति घर में घूम-फिर रहे हैं। अपनी सादगी,प्रसन्नता, स्नेहशीलता और सहज रूप से घुलमिल जाने की कुशलता के कारण डॉक्टर साहब कहीं भी अनचाहे नहीं हुए। स्वयंसेवकों में भी ये गुण वे देखना चाहते थे। 1939 में दूसरा विश्वयुद्ध भड़क उठा था और भारत की गुलामी का जुआ उखाड़ फेंकने के लिए एक सुनहरा अवसर सामने दिखाई दे रहा था। किन्तु इस मौके का लाभ उठाने के लिए आवश्यक संगठित राष्ट्रीय शक्ति थी कहाँ? ऐसी शक्ति खड़ी करने के लिए डॉक्टर साहब ने संघ-स्थापना से लेकर आज तक बिना रुके काम किया था।
सन् 1940 का अप्रेल का महीना आया। डॉक्टर साहब को पुणे के प्रशिक्षण-वर्ग की चिन्ता लगी। वे नागपुर आये और तुरन्त पुणे रवाना हो गये। तबियत नरम ही थी, फिर भी उन्होंने पुणे-वर्ग के सारे कार्यक्रम अत्यन्त उत्साह के साथ निपटाये। सब स्वयंसेवकों से व्यक्तिश: परिचय किया। पीठ का दर्द कष्ट दे ही रहा था। भारी गर्मी में भी उन्हें ठंड सहन नहीं होती थी। इसलिए ऊनी कपड़े सदा पहने रहना पड़ता था। फिर भी पुणे के पन्द्रह दिनों के कार्यक्रम वे सम्पन्न करते जा रहे थे। उन्होंने किसी को अपनी अस्वस्थता का पता नहीं लगने दिया। पुणे का शिक्षा-वर्ग समाप्त हुआ और स्वयंसेवको से उन्होंने प्रेमपूर्वक विदा ली। किन्तु उन्हें विदा देते समय कौन जानता था कि यह उनकी अंतिम विदाई है ? डाक्टर साहब ने श्री गुरुजी को पास बुलाकर सबके सामने उनसे कहा कि “अब संगठन का भार आपके कंधो पर है।" वे समझ गये थे कि अब उनके जीवन के दिन पूरे हो रहे हैं, इसलिए इस प्रकार आगे की व्यवस्था करके वे महायात्रा के लिए तैयार हो गये। आखिरकार उस असहनीय वेदना और सीमा के बाहर जाते ज्वर के सामने डाक्टर साहब को हाथ टेकने पड़े। 21 जून को प्रात: काल 9 बजकर 28 मिनट पर डाक्टर साहब की आत्मा अनन्त आकाश में विलीन हो गयी। यह 5042 युगाब्द अर्थात् ईसवी सन् 1940 का दिन था। यह समाचार बिजली की गति से चारों ओर फैल गया। बाबा साहेब घटाटे के बंगले के सामने स्वयंसेवकों और नागरिकों के झुंड जमा होने लगे। ग्राम-ग्राम से कार्यकर्ता और स्वयंसेवक पहुँचने लगे। उनकी अन्तिम यात्रा में सम्मिलित शोकाकुल समाज सड़क पर एक मील दूर तक फैला हुआ था। अनेकों की आँखों से अश्रुधारा बह रही थी। जिसने अपना कोई घरबार नहीं बसाया, उस राष्ट्र समर्पित महापुरुष के अंतिम दर्शनों के लिए भीड़ उमड़ रही थी। साथ में जब वर्षा की फुहारें भी पड़ीं तो ऐसा लगा मानो इन्द्रदेव भी लोगों के दु:ख में सम्मिलित हो गये हैं। डाक्टर साहब ने संघ के लिए रेशिमबाग में एक जगह खरीदी थी। वहीं उनका अंतिम संस्कार किया गया। उसी तपोभूमि पर आज उनका प्रेरणास्पद-स्मृति मंदिर खड़ा है।